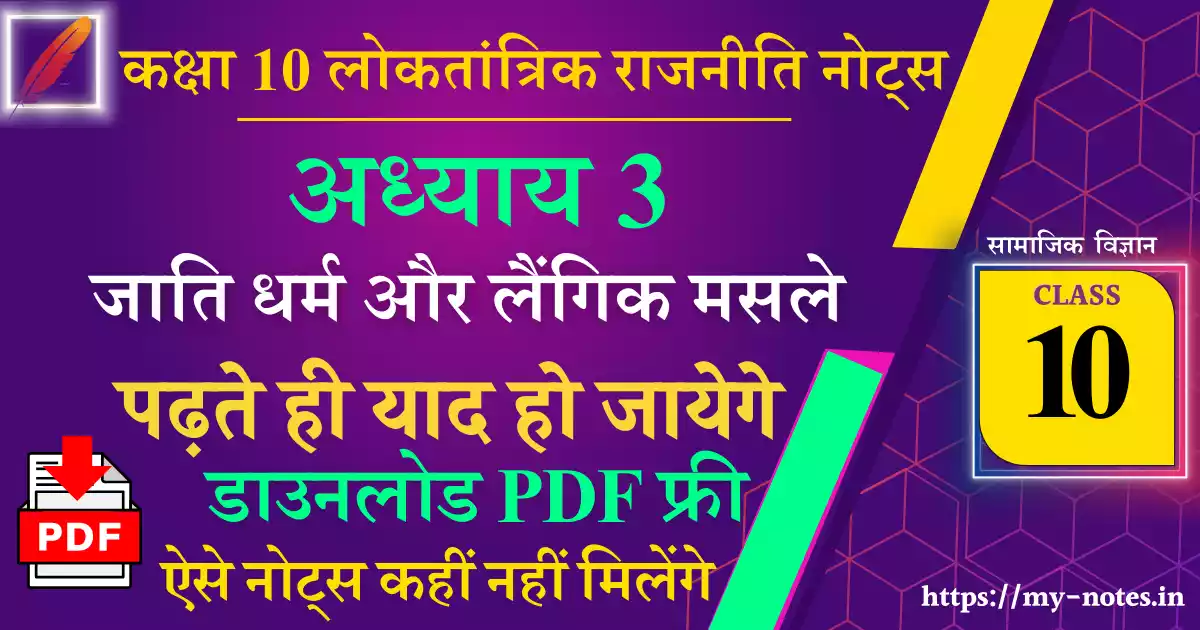प्रिय विद्यार्थियों आप सभी का स्वागत है आज हम आपको सत्र 2024-25 के लिए Class 10 लोकतांत्रिक राजनीति Chapter 3 जाति धर्म और लैंगिक मसले Notes PDF in Hindi कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान नोट्स हिंदी में उपलब्ध करा रहे हैं |Class 10 Samajik Vigyan Ke Notes PDF Hindi me Chapter 3 Jaati dharm owr laingik masale Notes PDF
Class 10 लोकतांत्रिक राजनीति Chapter 3 जाति धर्म और लैंगिक मसले Notes PDF in Hindi
Class 10 Social Science [ Class 10 Social Science Civics (Political Science): Democratic Politics-II ] Loktantrik Rajniti Chapter 3 Jaati dharm owr laingik masale Notes In Hindi
class-10-loktantrik-rajniti-chapter-3 gender-religion-and-caste-federalism-notes-pdf-in-hindi
10 Class लोकतांत्रिक राजनीति Chapter 3 जाति धर्म और लैंगिक मसले Notes in Hindi
| Textbook | NCERT |
| Class | Class 10 |
| Subject | लोकतांत्रिक राजनीति Political Science |
| Chapter | Chapter 3 |
| Chapter Name | जाति धर्म और लैंगिक मसले |
| Category | Class 10 राजनीति Notes in Hindi |
| Medium | Hindi |
अध्याय = 2
संघवाद
Class 10 सामाजिक विज्ञान
नोट्स
जाति धर्म और लैंगिक मसले
श्रम का लैंगिक विभाजन
लिंग के आधार पर विभाजन से तात्पर्य है:– अलग-अलग कार्यो का विभाजन अथवा वह व्यवस्था जिसमे सभी घरेलू कार्य घर की महिलाओं द्वारा किए जाते हैं और पैसे कमाने का कार्य पुरुषों को दिया गया है। अर्थात कार्यो का विभाजन करते समय लिंग को ध्यान में रखा जाता है, व्यक्ति की योग्यता को नहीं।
लिंग के आधार पर काम का बँटवारा। श्रम का लैंगिक विभाजन एक कटु सत्य है जो हमारे घरों और समाज में प्रत्यक्ष दिखाई देता है। घर के कामकाज महिलाओं द्वारा किए जाते हैंं या महिलाओं की देखरेख में नौकरों द्वारा किए जाते हैंं। पुरुषों द्वारा बाहर के काम काज किए जाते हैंं। एक ओर जहाँ सार्वजनिक जीवन पर पुरुषों का वर्चस्व रहता है वहीं दूसरी ओर महिलाओं को घर की चारदीवारी में समेट कर रखा जाता है।
नारीवादी आंदोलन:-
इन आंदोलनों में मुख्य रूप से महिलाओं को वैधानिक अधिकार दिए जाने पर बल दिया जाता है। जैसे- महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार मिलना, महिलाओं को वोट देने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, बौद्धिक रूप से समानता का अधिकार इत्यादि।
- महिलाओं को समान अधिकार दिलाने के उद्देश्य से होने वाले आंदोलन को नारीवादी आंदोलन कहते हैंं।
- हाल के वर्षों में लैंगिक मसलों को लेकर राजनैतिक गतिविधियों के कारण सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की स्थिति काफी सुधर गई है। भारत का समाज एक पितृ प्रधान समाज है। इसके बावजूद आज महिलाएँ कई क्षेत्रों में आगे बढ़ रही हैं। महिलाओं को अभी भी कई तरह के भेदभावों का सामना करना पड़ता है। जैसे- असमान लिंगानुपात, महिलाओं की औसत आयु में कमी और मृत्युदर की अधिकता के लिए बाल विवाह, प्रसवकाल में मृत्यु, महिलाओं की आर्थिक निर्भरता, लड़कियों की तुलना में लड़कों को अधिक महत्व देना, कुपोषण, स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव इत्यादि।
इसके कुछ उदाहरण नीचे दिये गए हैं:-
- पुरुषों में 76% के मुकाबले महिलाओं में साक्षरता दर केवल 54% है।
- ऊँचे पदों पर महिलाओं की संख्या काफी कम है ।
- कई मामलों में ये भी देखा गया है कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं को कम वेतन मिलता है। जबकि पुरुषों की तुलना में महिलाएँ प्रतिदिन अधिक घंटे काम करती हैं।
- आज भी अधिकाँश परिवारों में लड़कियों के मुकाबले लड़कों को अधिक प्रश्रय दिया जाता है।
- ऐसे कई मामले देखने को मिलते हैंं जिसमें कन्या को भ्रूण अवस्था में ही मार दिया जाता है।
- भारत का लिंग अनुपात महिलाओं के पक्ष में दूर-दूर तक नहीं है। महिलाओं पर होने वाले अत्याचार के कई मामले सामने आते हैंं और ये घटनाएँ घर में और घर के बाहर भी होती हैं।
नारीवादी आंदोलनों की आवश्यकता:-
नारीवादी आंदोलनों की आवश्यकता औरतों की सामाजिक स्थिति में सुधार लाने के लिए, शिक्षा के लिए, मतदान के लिए महिलाओं की राजनीतिक स्थिति एवं सामाजिक स्थिति में सुधार लाने के लिए है। इन आंदोलनों में महिलाओं के राजनीतिक और वैधानिक दर्जे को ऊँचा उठाने और उनके लिए शिक्षा तथा रोजगार के अवसर बढ़ाने की माँग की गई मूलगामी बदलाव की माँग करने वाली महिला आंदोलनों ने औरतों के व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में भी बराबरी की माँग उठाई।
10 Class लोकतांत्रिक राजनीति Chapter 3 जाति धर्म और लैंगिक
Class 10 सामाजिक विज्ञान
नोट्स
जाति धर्म और लैंगिक मसले
महिलाओं की भूमिका
समाज में महिलाओं की भूमिका:- वर्तमान समय में नारियों ने कृषि से लेकर अंतरिक्ष तक पुरुषों के बराबर स्थान ग्रहण किया है, लेकिन फिर भी आज के समय में भी ज्यादातर महिलाएँ मौलिक अधिकारों से वंचित है। महिला सशक्तिकरण के चाहे जितने भी प्रयास किए जा रहे हो लेकिन महिलाओं को चुनौती का सामना करना पड़ता है। महिलाओं को जन्म से ही अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे- भ्रूण हत्या, लैंगिक भेदभाव, घरेलू हिंसा, दहेज प्रथा, यौन उत्पीड़न, छेड़छाड़, शोषण, दमन, बलात्कार, मानसिक यंत्रणा इत्यादि।
- यह प्रचलित विश्वास है या चलन है कि औरतों का काम केवल बच्चों की देखभाल करना और घर की देखभाल करना है।
- उनके कार्य को ज्यादा मूल्यवान नहीं माना जाता है।
- आबादी में औरतो का हिस्सा आता है परंतु राजनीतिक जीवन या सामाजिक जीवन में उनकी भूमिका न के बराबर ही है।
सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भूमिका का परिद्यश्य बदल रहा है:– भारत में महिलाओं की स्थिति हमेशा एक जैसी नहीं रही है। इसमें समय के साथ-साथ बदलाव देखने को मिलता है। वर्तमान भारत में सार्वजनिक क्षेत्रों में महिलाओं का परिदृश्य बदल रहा है। महिलाएँ राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोक सभा अध्यक्ष, जैसे पदों पर आसीन हुई है। महिलाओं की स्थिति में सुधार ने देश के आर्थिक और सामाजिक मायने भी बदल कर रख दिए है।
- आज सार्वजनिक जीवन के परिदृश्य में औरतों की भूमिकाएँ काफी बदल गई हैं। वे एक वैज्ञानिक, डॉक्टर, शिक्षक आदि के रूप में सार्वजनिक जीवन में भूमिका निभाती दिखाई देती हैं।
- सार्वजनिक जीवन में औरतों की भागीदारी फिनलैंड, स्वीडन, नार्वे जैसे देशों में अधिक है।
महिलाओं के साथ भेदभाव तथा अत्याचार होते हैं:- समाज में महिलाओं की स्थिति में सुधार के बावजूद अनेक कारणों से उनके साथ भेदभाव और अत्याचार हो रहे है।
- महिलाओं में साक्षरता की दर 54% है जबकि पुरुषों में 76%।
- इसी प्रकार अब भी स्कूल पास करने वाली लड़कियों की एक सीमित संख्या ही उच्च शिक्षा की ओर कदम कदम बढ़ा पाई है क्योंकि माँ बाप लड़कियों की जगह लड़कों की शिक्षा पर ज्यादा खर्च करना पसंद करते हैं।
- उच्च पदों तक बहुत ही कम महिलाएँ पहुँच पाई है। उच्च भुगतान अनुपात में औरतों की संख्या बहुत ही कम है। अभी महिला सांसदों की लोकसभा में संख्या 100% तक नहीं पहुँची और प्रांतीय विधानसभाओं में उनकी संख्या 50% से भी कम है।
- महिलाओं को ज्यादातर काम पैसे के लिए नहीं मिलते, पुरुषों की अपेक्षा उनको मजदूरी भी कम मिलती है, भले ही दोनों ने समान कार्य किया हो।
- लड़की का जन्म परिवार पर एक बोझ समझा जाता है क्योंकि उसे जन्म से लेकर मृत्यु तक परिवार को कुछ न कुछ देना ही पड़ता है। शिक्षा के क्षेत्र में भी लड़कियों से भेदभाव किया जाता है। जहाँ लड़कों को जीवन यापन करने के लिए कोई न कोई काम सिखाया जाता है वही लड़कियों को रसोई तक ही सीमित रखा जाता है।
पितृ प्रधान समाज:-
हमारा समाज पुरूष प्रधान समाज है। दिन प्रतिदिन महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है, इसके बावजूद महिलाएँ अभी भी पीछे हैं। इसलिए हमारे समाज को पितृ प्रधान समाज माना जाता है।
पाठ 3 – जाति, धर्म और लैंगिक मसले लोकतांत्रिक राजनीति के नोट्स
Class 10 सामाजिक विज्ञान
नोट्स
जाति धर्म और लैंगिक मसले
निजी और सार्वजनिक विभाजन
निजी और सार्वजनिक विभाजन:- लैंगिक विभाजन से तात्पर्य है स्त्रियों और पुरुषों के बीच जैविक अंतर, समाज द्वारा प्रदान की गई स्त्रियों और पुरुषों की आसमान भूमिकाएँ, बालक एवं बालिकाओं की संख्या का अनुपात, लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाओं में महिलाओं को वोट का अधिकार न मिलना।
- श्रम के लैंगिक विभाजन अधिकतर महिलाएँ अपने घरेलू काम के अतिरिक्त अपनी आमदनी के लिए कुछ न कुछ काम करती हैं लेकिन उनके काम को ज्यादा मूल्यवान नहीं माना जाता और उन्हें दिन रात काम करके भी उसका श्रेय नहीं मिलता।
- मनुष्य जाति की आबादी में औरतों का हिस्सा आधा है पर सार्वजनिक जीवन में खासकर राजनीति में उनकी भूमिका नगण्य ही है।
- विभित्र देश में महिलाओं को वोट का अधिकार प्रदान करने के लिए आंदोलन हुए। इन आंदोलनों को नारीवादी आंदोलन कहा जाता है।
जीवन के विभिन्न पहलू जिनमें भारत में स्त्रियों के साथ भेदभाव होता है वे निम्नलिखित हैं:
- समाज में महिलाओं का निम्न स्थान- भारतीय समाज में महिला को सदा पुरुष से निम्न ही रखा गया है उससे कभी भी स्वतंत्र रूप से रहने का अवसर नहीं दिए गए हैं। कानूनी रूप से तो महिला और पुरुषोंं को समान अधिकार प्रदान कर दिए गये है, परन्तु सही मायने में हमारा समाज परम्पराओं को तोड़ने के लिए तैयार नहीं है। महिलाओं के प्रति जो बदलाव हो भी रहा है, उसकी गति बहुत धीमी है।
- बालिकाओं के प्रति उपेक्षा– आज भी बालिकाओं की अनेक प्रकार से अवहेलना की जाती है लड़के के जन्म पर आज भी सभी बड़े खुश होते हैं और अन्य जश्न मनाते हैं परन्तु लड़की के जन्म पर परिवार में चुपचाप हो जाता है दूसरी लड़की का जन्म परिवार पर एक बोझ समझा जाता क्योंकि उसे जन्म से लेकर मिलते हैं तो परिवार को कुछ न कुछ देना ही पड़ता है तीसरे शिक्षा के क्षेत्र में भी लड़कियों से भेदभाव किया जाता है चौथे जबकि लड़कों का जीवन यापन के लिए कोई न कोई काम सिखाया जाता है लड़कियों को रसोई तक ही सीमित रखा जाता है।
- पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं की दशा- आज भी हमारे समाज में सभी क्षेत्रों में निपुण होने के बावजूद महिलाएँ पुरुषों से पीछे है। पुरुष प्रधान समाज में महिला को पुरुषोंं से कम महत्व दिया जाता है। सरकार द्वारा महिलाओं के प्रति जागरूकता और कार्यक्रम चलाने के बाद भी महिला की ज़िन्दगी पुरुषोंं के मुकाबले काफी जटिल है तथा निम्नलिखित कारणों के आधार पर उनके साथ भेदभाव किया जाता है।
- साक्षरता दर के आधार पर
- ऊँची तनख्वाह वाले और ऊँचे पदों पर पहुँचने वाली महिलाओं की संख्या कम है
- महिलाओं के घर के काम को मूल्यवान नहीं माना जाता
- पुरुषोंं की तुलना में कम मजदूरी
- लड़की को जन्म लेने से पहले ही खत्म कर देना
- महिलाओं के उत्पीड़न, शोषण और उन पर होने वाली हिंसा।
जाति, धर्म और लैंगिक मसले Notes || Class 10 Social Science
Class 10 सामाजिक विज्ञान
नोट्स
जाति धर्म और लैंगिक मसले
सांप्रदायिकता
सांप्रदायिकता:- अपने धर्म को ऊँचा समझना तथा दूसरे धर्मों को नीचा समझना और अपने धर्म से प्यार करना और दूसरे धर्मों से घृणा करने की प्रवृत्ति को सांप्रदायिकता कहते हैं। इस प्रकार प्रजातंत्र के मार्ग में एक बड़ी बाधा उपस्थित हो जाती है देश का बटवारा इसी भावना का परिणाम था।
इस बुराई को निम्नलिखित विधियों से दूर किया जा सकता है:-
- शिक्षा द्वारा- शिक्षा के पाठ्यक्रम में सभी धर्मों को अच्छा बताया जाए और विद्यार्थियों को सहिष्णुता एवं सभी धर्मों के प्रति आदर भाव सिखाया जाए ।
- प्रचार द्वारा- समाचार-पत्र, रेडियो, टेलीविजन, आदि से जनता को धार्मिक सहिष्णुता की शिक्षा दी जाए।
- सभी धर्मो का सम्मान करना- सभी धर्मावलम्बियों को प्रेरित करना चाहिए कि अपने धर्म का पालन करने के साथ-साथ अन्य सम्प्रदायों का भी सम्मान करे तथा उन्हें आदर की दृष्टि से देखे।
- तुष्टिकरण की नीति का त्याग करना– शासन को तुष्टिकरण की नीति का परित्याग करना चाहिए।
धर्म, सांप्रदायिकता और राजनीति:-
धर्म हमारे राजनैतिक और सामाजिक जीवन का एक अभिन्न अंग है। जब राजनैतिक वर्गों के द्वारा एक धर्म के लोगों को दूसरे धर्म के लोगों से लड़वाया जाता है तो इसे साम्प्रदायिकता व सांप्रदायिक राजनीति कहते हैं।
- लैंगिक विभाजन के विपरीत धार्मिक विभाजन अक्सर राजनीति के मैदान में अभिव्यकत होता है।
- धार्मिक विभाजन को सम्प्रदायवाद कहते हैं। सम्प्रदायवाद के कारण देश में झगड़े होते हैं और शांति भंग होती है। ऐसे वातावरण में लोकतंत्र पनप नहीं सकता है।
- समुदायवाद के कारण देश के अंदर घृणा व मतभेद उत्पत्र होते हैं और देश की एकता समाप्त हो जाती हैं। इस प्रकार लोकतंत्र को खतरा पैदा हो जाता है।
- जब एक धर्म के विचारों को दूसरे से श्रेष्ठ माना जाने लगता है और कोई एक धार्मिक समूह अपनी माँगों को दूसरे समूह के विरोध में खड़ा करने लगता है। इस प्रक्रिया में जब राज्य अपनी सत्ता का इस्तेमाल किसी एक धर्म के पक्ष में करने लगता है तो स्थिति और विकट होने लगती है। राजनीति से धर्म और इस तरह जोड़ना ही सांप्रदायिकता या सम्प्रदायवाद है।
- लोकतंत्र की सफलता का आधार है जनता में सहनशीलता, साझेदारी, बंधुत्व, सभी के विचारों के प्रति सहिष्णुता आदि। परन्तु सम्प्रदायवाद के कारण इन सभी के मार्ग में बाधा उत्पत्र हो जाती है।
सांप्रदायिकता के रूप:- साम्प्रदायिकता के अनेक रूप हैं।
- एक धर्म को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ मानना।
- अलग राजनीतिक इकाई बनाने की इच्छा।
- धर्म के पवित्र प्रतिकों, धर्मगुरू ओं की भावनात्मक अपीलों का प्रयोग।
- संप्रदाय के आधार पर हिंसा, दंगा और नरसंहार।
धर्मनिरपेक्ष शासन:-
वह शासन जिसमे सभी धर्मो को समान समझा जाता हैं। भारत भी एक धर्मनिरपेक्ष राज्य हैं। 24वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन करके धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया हैं।
- भारत का संविधान किसी धर्म को विशेष दर्जा नहीं देता।
- किसी भी धर्म का पालन करने और प्रचार करने की आजादी।
- धर्म के आधार पर किए जाने वाले किसी तरह के भेदभाव को अवैधानिक घोषित।
- शासन को धार्मिक मामलों में दखल देने का अधिकार।
- संविधान में किसी भी तरह के जातिगत भेदभाव का निषेथ किया गया है।
लोकतांत्रिक राजनीति NCERT Book Class 10 PDF Download
Class 10 सामाजिक विज्ञान
नोट्स
जाति धर्म और लैंगिक मसले
जातिवाद
जातिवाद:– भारत में जाति व्यवस्था प्राचीन समय से ही विद्यमान है। प्राचीन समय में जाति के आधार पर समाज चार वर्गों में विभाजित किया गया था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, एवं शूद्र।
जाति प्रथा आज भी भारतीय समाज का अभित्र अंग है। समय समय पर इसमें अनेक बदलाव आते गए और इसे सुधारने का प्रयत्न किया गया। भारतीय संविधान ने किसी भी प्रकार के जातिगत भेदभाव का निश्चित किया है और जाति व्यवस्था से पैदा होने वाले अन्याय को समाप्त करने पर जोर दिया है। परन्तु इतना सब कुछ होते हुए भी समकालीन भारत में जाति प्रथा विद्यमान है।
जाति व्यवस्था के कुछ पुराने पहलू आज भी विद्यमान है। अभी भी अधिकतर लोग अपनी जाति या कबीले में नहीं विवाह करते हैं सदियों से जिन जातियों का पढ़ाई लिखाई के क्षेत्रों में प्रभुत्व स्थापित था वह आज भी है और आधुनिक शिक्षा में उन्हीं का बोल बाला है। जिन जातियों को पहले शिक्षा से वंचित रखा गया था उनके सदस्य अभी तक स्वाभाविक रूप से पिछड़े हुए हैं।
जिन लोगों का आर्थिक क्षेत्र में प्रभुत्व स्थापित था वे आज भी थोड़े बहुत अंतर के बाद मौजूद है। जाति और आर्थिक हैसियत मे काफी निकट का संबंध माना जाता है। देश में सवैधानिक प्रावधान के बावजूद युवा छोटी प्रथा अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई है।
जाति पर आधारित आंदोलन:-
स्वतन्त्रता के बाद भारत में जाति पर आधारित अनेक आंदोलन चलाये गये। जैसे-1 उन्नीसवीं सदी में ज्योतिराव फुले द्वारा निम्न जाति के उत्थान के लिए शुरू किया गया आंदोलन। 2 डॉ.भीमराव.अम्बेडकर द्वारा 1920 और 1930 के बीच एक महत्वपूर्ण दलित आंदोलन शुरू किया गया | उन्होंने भारत में दलितों की दशा सुधारने के लिए स्वतंत्र भारत में आरक्षण की एक प्रणाली बनाई।
राजनीति में जाति:
– जाति व्यवस्था किसी न किसी रूप में विश्व के प्रत्येक क्षेत्रों में पायी जाती है बाबू जगजीवन राम के अनुसार जाति भारतीय राजनीति की सर्वाधिक महत्वपूर्ण सत्यता है एक सामान्य भारतीय अपना सबकुछ त्याग सकता है परन्तु जाति व्यवस्था में अपने विश्वास की तिलांजलि नहीं दे सकता है। जाति प्रथा भारतीय हिन्दू समाज की प्रमुख विशेषताएँ है-
- चुनाव क्षेत्र के मतदाताओं की जातियों का हिसाब ध्यान में रखना।
- समर्थन हासिल करने के लिए जातिगत भावनाओं को उकसाना।
- देश के किसी भी एक संसदीय चुनाव क्षेत्र में किसी एक जाति के लोगों का बहुमत नहीं है।
- कोई भी पार्टी किसी एक जाति या समुदाय के सभी लोगों का वोट हासिल नहीं कर सकती।
जातिगत असामनता:-
जाति के आधार पर आर्थिक विषमता अभी भी देखने को मिलती है। ऊँची जाति के लोग सामन्यतया संपत्र होते है। पिछड़ी जाति के लोग बीच में आते हैं और दलित तथा आदिवासी सबसे नीचे आते हैं। सबसे निम्न जातियों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या बहुत अधिक है।
Political Science 3 जाति , धर्म और लैंगिक मसले Class-10
प्रश्न1. समाज द्वारा स्त्री और पुरुष को दी गई असमान भूमिकाएँ क्या कहलाती हैं?
उत्तर – लैंगिक विभाजन।
प्रश्न2. भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किन प्रतिनिधि संस्थाओं में है?
उत्तर – पंचायती राज की संस्थाओं में।
प्रश्न3. 2001 की जनगणना के अनुसार भारत के किन राज्यों में लिंगानुपात 900 से भी कम है?
उत्तर – पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और सिक्किम।
प्रश्न4. स्थानीय सरकारों में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था है?
उत्तर – 33 प्रतिशत।
प्रश्न5. लिंगानुपात किसे कहते हैं?
उत्तर – प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या।
प्रश्न6. धर्म को राजनीति से कभी भी अलग नहीं किया जा सकता – ये शब्द किसने कहे हैं?
उत्तर – महात्मा गाँधी।
प्रश्न7. एक ऐसे समुदाय के लोग जो साधारण तया पहाड़ी और जंगली क्षेत्रों में रहते हैं और जिनकी बाकी समाज से अधिक मेल जोल नहीं है, क्या कहते हैं?
उत्तर – अनुसूचित जनजाति।
प्रश्न8. उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें लोग ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की और पलायन करते हैं?
उत्तर – शहरीकरण।
प्रश्न9. जीवन में उन विभिन्न पहलुओं का जिक्र करें जिनमें भारत में स्त्रियों के साथ भेदभाव होता है।
उत्तर – जीवन में उन विभिन्न पहलुओं का जिक्र इस प्रकार से जिनमें भारत में स्त्रियों के साथ भेदभाव होता है –
1. महिलाओं के ऊपर पूरा घरेलू दायित्व।
2. पुरुषों का अत्यधिक नियंत्रण।
3. व्यवस्थापिकाओं में कम प्रतिनिधित्व।
4. कन्या भ्रूण हत्या
5. स्त्री शिक्षा को कम महत्व।
6. पारिश्रमिक वितरण में असमानता।
प्र10. जाति के आधार पर भारत में चुनावी नतीजे तय नहीं किये जा सकते कारण लिखिए।
उत्तर – जाति के आधार पर भारत में चुनावी नतीजे तय नहीं किये जा सकते कारण निम्न –
✫ मतदाताओं में जागरूकता – कई बार मतदाता जातीय भावना से ऊपर उठकर मतदान करते हैं।
✫ मतदाताओं द्वारा अपने आर्थिक हितों और राजनीतिक दलों को प्राथमिकता।
✫ किसी एक संसदीय क्षेत्र में किसी एक जाति के लोगों का बहुमत न होना।
✫ मतदाताओं द्वारा विभिन्न आधारों पर मतदान करना।
NCERT Class 6 to 12 Notes in Hindi
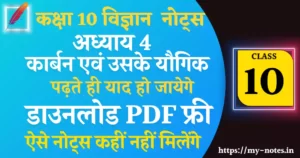
प्रिय विद्यार्थियों आप सभी का स्वागत है आज हम आपको Class 10 Science Chapter 4 कार्बन एवं उसके यौगिक Notes PDF in Hindi कक्षा 10 विज्ञान नोट्स हिंदी में उपलब्ध करा रहे हैं |Class 10 Vigyan Ke Notes PDF
URL: https://my-notes.in/
Author: NCERT
5
Pros
- Best NCERT Notes in Hindi